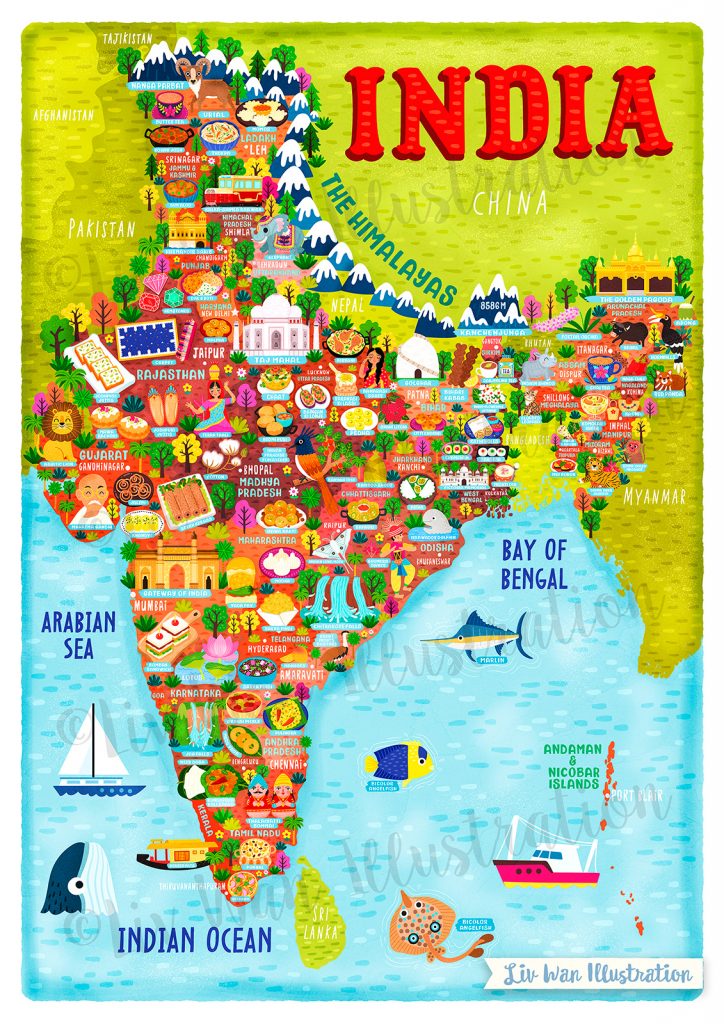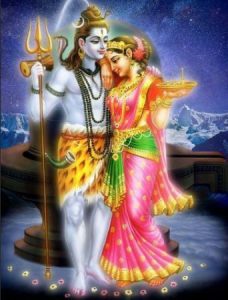उज्जैन,( आलेख:- कनिष्क सिंह भदौरिया ) पिछले तीन दशकों से भारत ने वैश्वीकरण की राह पर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाया है। 1991 के उदारीकरण सुधारों के बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, विदेशी पूंजी को आकर्षित किया और वैश्विक बाज़ार का हिस्सा बने। लेकिन हाल ही में माहौल में एक बदलाव महसूस हो रहा है शुरुआत में यह परिवर्तन सूक्ष्म था, लेकिन अब इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल होता जा रहा है।
क्या भारत फिर से अपने भीतर सिमट रहा है? क्या हम आर्थिक संरक्षणवाद के एक नए युग को अपना रहे हैं? यह सवाल आज के बदले हुए विश्व परिदृश्य में और भी प्रासंगिक हो जाता है।
संरक्षणवादी राज्य की वापसी
पहले समझते हैं संरक्षणवाद क्या है। इसका मूल भाव है घरेलू उद्योगों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाना। इसके लिए सरकारें आयात शुल्क बढ़ाती हैं, सब्सिडी देती हैं, या विदेशी निवेश पर सख्ती करती हैं। यह कोई नया विचार नहीं है। सदियों से राष्ट्र इसे अपनाते आए हैं, राष्ट्रीय हित या आर्थिक संप्रभुता के नाम पर लेकिन एक वैश्वीकृत दुनिया में, संरक्षणवाद पिछली सदी की बात लगने लगी थी। फिर आई महामारी, फिर यूक्रेन युद्ध और फिर बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव। अचानक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता एक कमजोरी लगने लगी।
देश पीछे हटने लगे। अमेरिका ने अपने सेमीकंडक्टर और ईवी उद्योग को सब्सिडी देनी शुरू की। यूरोप ने “रणनीतिक आत्मनिर्भरता” की बात छेड़ी। और भारत? हमने शुरू किया आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसे कई लोग रणनीतिक संरक्षणवाद के भारतीय संस्करण के रूप में देखते हैं।
आज भारत में संरक्षणवाद कैसा दिखता है?
यह कहना कि भारत संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहा है, कोई आरोप नहीं बल्कि एक विश्लेषण है। और शायद यह रणनीतिक रूप से आवश्यक भी है।
हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, फर्नीचर, मोबाइल फोन जैसी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। संदेश साफ़ है “भारत में बनाओ, बाहर से मत मंगाओ।”
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाएं इसका एक और उदाहरण हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय निर्माताओं को अकेला छोड़ने के बजाय, सरकार उन्हें प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दे रही है ताकि वे अपने पैमाने और क्षमताओं को बढ़ा सकें। फार्मा से लेकर सोलर पैनलों तक कई क्षेत्रों में घरेलू क्षमता विकसित करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। इसके साथ ही चीन पर निर्भरता घटाने की एक शांत लेकिन ठोस कोशिश भी हो रही है। 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद, चीन की कई मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा, निवेश पर सख्ती हुई, और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और API (सक्रिय फार्मास्युटिकल तत्व) में विकल्प तलाशे जाने लगे। यहां तक कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी FDI नियम बदले गए, ताकि “सांस्कृतिक निकटता वाले देशों” से आने वाले निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के “अवसरवादी अधिग्रहण” को रोका जा सके।
लचीलापन बनाम अलगाव
संरक्षणवाद के साथ जोखिम भी आते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां उद्योगों को इतने अधिक संरक्षित किया गया कि वे कभी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन ही नहीं पाए। शुल्कों से आत्मसंतोष बढ़ सकता है, और सब्सिडी यदि लंबे समय तक चलें तो उद्योग उनका सहारा लेने लगते हैं।
तो असली सवाल है: क्या हम दीर्घकालिक क्षमताएं बना रहे हैं या सिर्फ तात्कालिक राहत खरीद रहे हैं?
आदर्श स्थिति होगी एक रणनीतिक संरक्षणवाद जो नवाचार को प्रोत्साहन दे, रोजगार बनाए, आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करे, और वैश्विक व्यापार से पूरी तरह कटे बिना भारत को आत्मनिर्भर बनाए।
संतुलन की डगर पर भारत
वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति जटिल है। WTO में हम अब भी किसानों, लघु उद्योगों और समावेशी विकास के हित में सुरक्षा की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर, हम यूके, ऑस्ट्रेलिया और EU जैसे देशों से व्यापार समझौते भी कर रहे हैं जिसमें घरेलू हित और वैश्विक आकांक्षाओं के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। यही समय को रोचक बनाता है। हम वैश्वीकरण को नकार नहीं रहे हैं बल्कि इसके साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। अब हम केवल एक निष्क्रिय सहभागी नहीं रहना चाहते, बल्कि वैश्विक नियमों को अपने हित में ढालना चाहते हैं।
तो क्या यह सही दिशा है?
इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। संरक्षणवाद एक प्रभावशाली साधन हो सकता है या एक खतरनाक प्रलोभन। यह नवाचार को जन्म दे सकता है या उसे कुचल भी सकता है। लेकिन आज की अनिश्चित दुनिया में, शायद सही सवाल यह नहीं कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए या नहीं बल्कि यह है कि कैसे करें और कब तक करें। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ वैश्विक तूफानों में टिके रहना नहीं है — बल्कि अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना है।